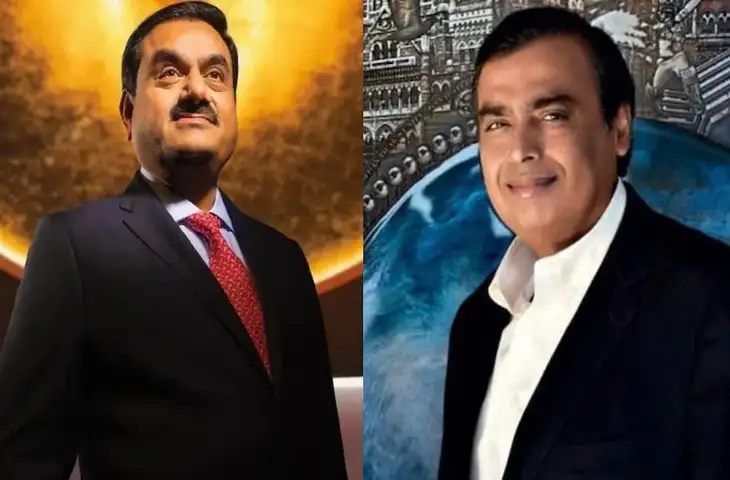इस खबर को सुनने के लिये प्ले बटन को दबाएं।
इस खबर को सुनने के लिये प्ले बटन को दबाएं।



भारत की तस्वीर तेजी से बदल रही है। गांवों से शहरों की ओर पलायन ने देश के शहरी क्षेत्रों को लगातार विस्तार दिया है। यूनाइटेड नेशन (UN) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2050 तक भारत की 53% से ज्यादा आबादी शहरों में रहने लगेगी। यह संख्या आज की तुलना में लगभग दोगुनी होगी।
लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत के शहर इस बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए तैयार हैं? क्या शहरों की सड़कें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक सिस्टम इस दबाव को झेल पाएंगे?
दुर्भाग्य से, जवाब ‘नहीं’ की तरफ झुकता है।
तेजी से फैलते शहर, लेकिन धीमी योजना
पिछले दो दशकों में दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद और जयपुर जैसे शहरों का भूगोल तेजी से बढ़ा है। नई कॉलोनियां और टाउनशिप तो विकसित हो रही हैं, पर उनके बीच ट्रांसपोर्ट का ढांचा कमजोर है।
नई सड़कें बन तो रही हैं, लेकिन उनका जुड़ाव (connectivity) योजना के अनुसार नहीं है। कई इलाकों में मेट्रो स्टेशन दूर हैं, बसें सीमित हैं, और ऑटो-टैक्सी के दाम आसमान छूते हैं।
अर्बन प्लानिंग में अक्सर हाउसिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन अर्बन ट्रांसपोर्ट को समान महत्व नहीं मिलता।
यही कारण है कि शहरी विस्तार के साथ-साथ ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और समय की बर्बादी भी बढ़ती जा रही है।
अर्बन ट्रांसपोर्ट से कटी अर्बन प्लानिंग
भारत में कई शहरों में मास्टर प्लान तो बनाए जाते हैं, पर उनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम को समग्र रूप से नहीं जोड़ा जाता।
उदाहरण के तौर पर, किसी नए आवासीय क्षेत्र का विकास तो किया जाता है, लेकिन वहां तक पहुँचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा बाद में सोची जाती है।
यही कारण है कि शहरों में निजी वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।
दिल्ली में हर महीने करीब 75,000 नए वाहन पंजीकृत हो रहे हैं।
इसी तरह मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों में ट्रैफिक का दबाव अपने चरम पर है।
अर्बन ट्रांसपोर्ट की अनुपस्थिति में आम नागरिक को या तो निजी वाहन लेना पड़ता है या फिर ट्रांसपोर्ट माफिया के शिकंजे में फंसना पड़ता है।
ट्रांसपोर्ट माफिया का कब्जा
जब सरकारी बसें कम चलती हैं, मेट्रो हर इलाके में नहीं पहुंचती और टैक्सी सेवाएं महंगी होती हैं — तब बीच का रास्ता निकलता है अनियमित निजी परिवहन।
शहरों में छोटे-छोटे निजी ऑपरेटर, ई-रिक्शा और लोकल वैन ड्राइवर बिना लाइसेंस या नियंत्रण के चलने लगते हैं।
ये “ट्रांसपोर्ट माफिया” केवल किराया बढ़ाकर जनता को लूटते ही नहीं, बल्कि शहर की यातायात व्यवस्था को भी अव्यवस्थित कर देते हैं।
उनकी मनमानी से ट्रैफिक जाम और सड़क हादसे बढ़ते हैं, जबकि यात्री सुरक्षा का कोई मानक नहीं रहता।
स्मार्ट सिटी मिशन की सीमाएं
सरकार ने “स्मार्ट सिटी मिशन” की शुरुआत इसी सोच के साथ की थी कि शहरों को तकनीक और योजना से सुसज्जित किया जाए।
हालांकि, अब तक जिन शहरों में यह मिशन लागू हुआ है, वहां भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्राथमिकता नहीं मिली है।
कई जगह मेट्रो रेल प्रोजेक्ट तो शुरू हुए हैं, लेकिन वे केवल मुख्य इलाकों तक सीमित हैं।
लास्ट माइल कनेक्टिविटी यानी अंतिम पड़ाव तक यातायात सुविधा न होने से नागरिकों को परेशानी झेलनी पड़ती है।
अंतरराष्ट्रीय उदाहरण से सीख
जापान, सिंगापुर, और यूरोपीय देशों ने शहरी परिवहन की समस्या का समाधान पहले ही ढूंढ लिया है।
वहां शहरों का विकास “Transit-Oriented Development (TOD)” के सिद्धांत पर किया जाता है — यानी जहां परिवहन, आवास और वाणिज्यिक क्षेत्रों की योजना साथ-साथ बनाई जाती है।
भारत में भी यदि इस मॉडल को अपनाया जाए, तो ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और ऊर्जा की खपत में भारी कमी आ सकती है।
पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर असर
असंगठित ट्रांसपोर्ट व्यवस्था का सीधा असर पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ता है।
बढ़ते निजी वाहनों से कार्बन उत्सर्जन में तेजी आई है।
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 102 शहर “गंभीर वायु प्रदूषण” की श्रेणी में आते हैं — जिनमें से 70% प्रदूषण ट्रैफिक से जुड़ा है।
आर्थिक दृष्टि से देखें तो, ट्रैफिक जाम और परिवहन में देरी के कारण भारत को हर साल लाखों करोड़ रुपये का नुकसान होता है।
बिजनेस और कार्यस्थलों तक पहुंचने में लगने वाला अतिरिक्त समय उत्पादकता पर बुरा असर डालता है।